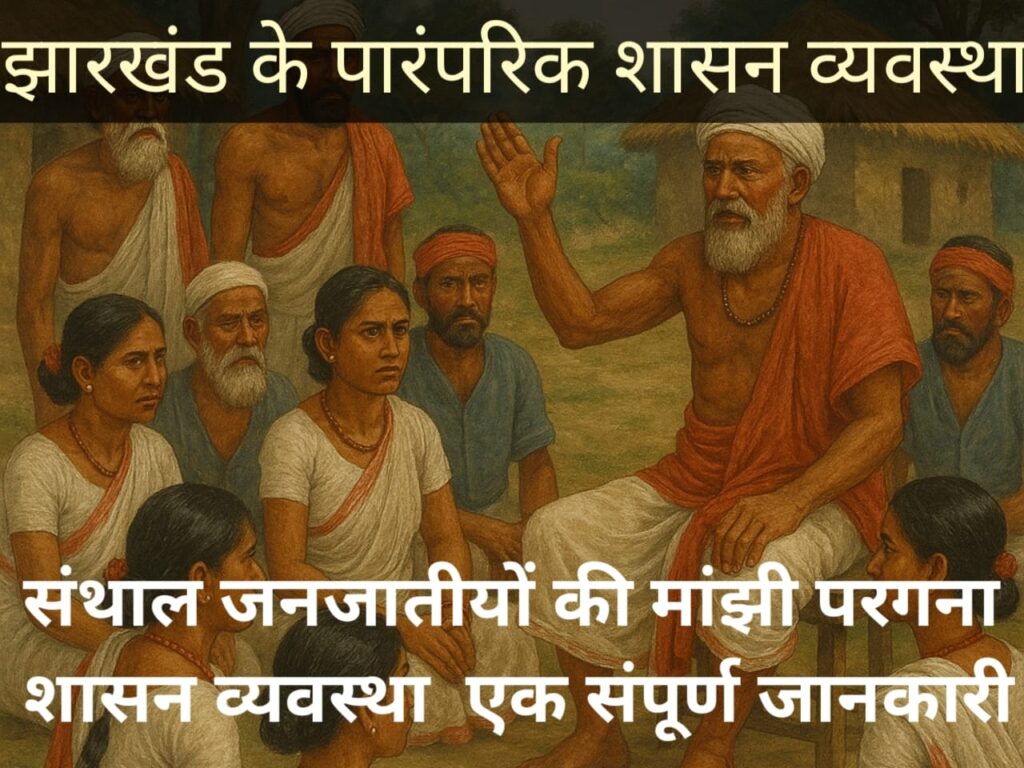संथाल भारत की एक प्रमुख जनजाति है, जो व्यवस्थित कृषि करने के लिए जानी जाती है। झारखंड की जनजातियों में संथालों की संख्या सबसे अधिक है, और उनका प्रमुख निवास क्षेत्र संथाल परगना माना जाता है। माना जाता है कि संथाल, झारखंड आने से पहले एक लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में निवास करते थे, जहाँ उन्हें ‘साओतार’ कहा जाता था। वहीं से वे संथाल परगना क्षेत्र में आकर बसे।संथाल परगना के पहले से बसे हुए लोग पहाड़िया समुदाय से थे। जब 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, तो पहाड़िया जनजाति ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता-प्रिय पहाड़िया जनजाति को काबू में लाने में असफल अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने संथालों और पहाड़ियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके परिणामस्वरूप, 1832-33 में लगभग 1338 वर्गमील क्षेत्र को सीमांकित कर एक विशेष क्षेत्र, ‘दामिन-ए-कोह’, की स्थापना की गई। यह क्षेत्र मूलतः पहाड़िया जनजाति की भूमि थी, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ संथालों को बसाया गया। इस बसावट के साथ ही संथालों ने अपनी पारंपरिक सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ स्थापित किया, जिसमें माँझी शासन व्यवस्था (Manjhi system) प्रमुख थी। झारखंड राज्य की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपरागत सामाजिक व्यवस्थाओं से होती है। इनमें से संथाल समुदाय की स्वशासन प्रणाली सबसे संगठित और प्रभावशाली मानी जाती है। संथाल परगना क्षेत्र में माँझी शासन व्यवस्था (Manjhi system) व्यवस्था आज भी समाज को एकजुट रखने और न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाती है।
मांझी परगना शासन व्यवस्था (Manjhi system) में ग्राम स्तर पर पारंपरिक पदाधिकारी
1. मांझी (ग्राम प्रधान)
मांझी गांव का प्रमुख होता है। यह प्रशासन, न्याय और धार्मिक मामलों में गांव का नेतृत्व करता है। गांव के अंदर और बाहर होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी उसी की होती है।
2. प्रानीक (उप-मांझी)
मांझी की अनुपस्थिति में यह सभी कार्यों को संभालता है और किसी अपराध का दंड तय करने की भूमिका निभाता है।
3. गोड़ाईत (सचिव)
गांव में सूचना देने, चंदा इकट्ठा करने और पूजा-पाठ में सहायता करता है।
4. जोग मांझी (युवा प्रमुख)
शादी-ब्याह से जुड़े कार्यों का संचालन करता है और युवाओं का नेतृत्व करता है।
5. जोग प्रानीक
यह जोग मांझी का सहयोगी होता है।
6. भग्दो प्रजा
ये गांव के सम्मानित सदस्य होते हैं, जो बैठक में भाग लेते हैं और निर्णय प्रक्रिया में सहयोग करते हैं।
7. लासेर टैंगोय
यह गांव की बाहरी सुरक्षा का प्रभारी होता है।
8. नायके और कुड़ाम नायके
नायके गांव के भीतर देवी-देवताओं की पूजा करता है जबकि कुड़ाम नायके गांव के बाहर के धार्मिक स्थलों की पूजा करता है।
मांझी परगना शासन व्यवस्था (Manjhi system)के उच्च स्तरीय नेतृत्व
1. देश मांझी / मोड़े मांझी
ये कई गांवों के मांझियों का नेतृत्व करते हैं। जब किसी विवाद का समाधान गांव स्तर पर नहीं होता तो मामला इनके पास जाता है।
2. परगनैत
15-20 गांवों के मामलों का निपटारा करने वाला सर्वोच्च नेता होता है।
3. दिशुम परगना
कुछ क्षेत्रों में परगनैतों से ऊपर एक और पद होता है, जो असाधारण मामलों का निपटारा करता है।
मांझी परगना शासन व्यवस्था (Manjhi system)का न्याय प्रक्रिया
परंपरागत स्वशासन व्यवस्था में पारिवारिक एवं ग्राम स्तरीय विवादों का समाधान
झारखंड के आदिवासी समाज में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था आज भी सामाजिक समरसता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। गांव या परिवार के भीतर उत्पन्न विवादों को निपटाने के लिए यहां एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित है, जिसमें मांझी, प्रानीक, नायके आदि पदधारी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
विवाद की प्रारंभिक सूचना और गांव सभा की प्रक्रिया
किसी प्रकार के पारिवारिक या सामाजिक विवाद की स्थिति में सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति गांव के मांझी से संपर्क करता है। मांझी, अपनी जिम्मेदारी के तहत गांव के अन्य प्रमुख पदधारियों एवं ग्रामीणों को इस विवाद की जानकारी देकर सभा बुलाते हैं। यह सूचना प्रायः ‘गोड़ाईत’ के माध्यम से दी जाती है, जो परंपरागत संदेशवाहक की भूमिका निभाता है।
सभा में विचार और निर्णय प्रक्रिया
ग्रामसभा में शिकायतकर्ता, आरोपित पक्ष और यदि उपलब्ध हों तो गवाहों से क्रमवार बयान लिया जाता है। इसके बाद मांझी, प्रानीक, जोग मांझी, नायके, जोग प्रानीक और उपस्थित प्रजाजनों की सहभागिता से चर्चा की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध होता है, तो अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ‘प्रानीक’ द्वारा दंड निर्धारित किया जाता है।
दंड व्यवस्था की विशेषता
पारंपरिक व्यवस्था में दंड आर्थिक रूप में ही दिया जाता है। सबसे हल्के दंड को ‘करेला दंड’ कहा जाता है, जिसकी राशि पहले 1.50 रुपये से 5 रुपये तक होती थी, लेकिन समय के साथ इसमें वृद्धि की गई है। गंभीर अपराधों के लिए दंड की राशि भी अधिक होती है। यदि दोषी व्यक्ति दंड भरने की स्थिति में नहीं है, तो उसे समय भी दिया जाता है।
विवाद की ऊंची सीढ़ियाँ – देश मांझी और परगनैत की भूमिका
कुछ मामले ग्रामसभा में नहीं सुलझ पाते, या दोषी पक्ष दंड स्वीकार नहीं करता, तो मांझी ऐसे मामलों को ‘देश मांझी’ (या मोड़े मांझी) के पास भेजते हैं। यदि देश मांझी भी मामला सुलझाने में असमर्थ होते हैं, तो अंततः यह विवाद ‘परगनैत’ के पास जाता है, जो उससे संबंधित क्षेत्रीय स्तर के पारंपरिक प्रमुख होते हैं।
आपराधिक मामलों में पारंपरिक नेतृत्व का दखल
साधारण आपराधिक मामलों—जैसे चोरी, मारपीट, पारिवारिक हिंसा आदि—को पारंपरिक पंचायत में ही सुलझाया जाता है। हत्या जैसे गंभीर अपराध इस प्रक्रिया से बाहर माने जाते हैं। विशेष अवसरों पर ग्रामसभा में उपस्थित ‘जूरी’ को यह अधिकार होता है कि वे दंड की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करें। छोटे-मोटे झगड़े, जमीन-जायदाद के विवाद, यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों को पहले मांझी की सभा में सुना जाता है। यदि निर्णय से कोई असंतुष्ट हो, तो मामला क्रमश: देश मांझी, फिर परगनैत के पास भेजा जाता है। आर्थिक दंड से लेकर सामाजिक बहिष्कार (बिटलाहा) तक की सजाएँ दी जाती हैं। बिटलाहा सबसे कठोर दंड है, जिसमें दोषी का चूल्हा तोड़ दिया जाता है और पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है।
सामाजिक-धार्मिक भूमिका
पारंपरिक नेतृत्व की दृष्टि में यौन अपराध, अवैध संतान और बिटलाहा प्रथा
झारखंड के आदिवासी समाज में पारंपरिक न्याय प्रणाली केवल सामाजिक या पारिवारिक विवादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह यौन अपराध, अविवाहित मातृत्व और सामाजिक अनुशासन जैसे संवेदनशील विषयों पर भी अपना निर्णायक दृष्टिकोण रखती है। यह व्यवस्था अपराध की गंभीरता, सामाजिक मर्यादा और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है।
1. यौन अत्याचार या बलात्कार के मामलों में पारंपरिक न्याय प्रणाली की भूमिका
जब किसी महिला या किशोरी के साथ यौन हिंसा की घटना घटती है, तो सबसे पहले पीड़िता स्वयं या उसके अभिभावक गांव के मांझी से संपर्क करते हैं। मांझी इस संबंध में बैठक आयोजित करता है और आरोपी को उपस्थित करने की सूचना देता है।
बैठक में शिकायतकर्ता, आरोपी और साक्ष्यों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। यदि आरोपी दोषी सिद्ध होता है और पीड़िता एवं आरोपी दोनों विवाह के लिए सहमत हों, तो विवाह का प्रस्ताव दिया जाता है। किन्तु यदि आरोपी विवाह से इनकार करता है, तो मामला अगली उच्च पारंपरिक संस्था—देश मांझी—के पास भेज दिया जाता है।
यदि देश मांझी भी समाधान देने में असफल रहता है, तो यह मामला परगनैत के पास जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था संवेदनशील मामलों में भी एक क्रमबद्ध न्याय प्रक्रिया का पालन करती है।
2. अविवाहित मातृत्व और अवैध संतान संबंधी व्यवस्था
संताल समाज में यदि कोई अविवाहित युवती गर्भवती हो जाती है, तो सबसे पहले ‘जोग मांझी’ को इसकी सूचना दी जाती है। वह गांव में बैठक बुलाता है और लड़की से बच्चे के पिता का नाम पूछता है। यदि लड़की किसी युवक का नाम बताती है और यह बात गवाहों से प्रमाणित हो जाती है, तो उस युवक को लड़की सौंप दी जाती है।
परंतु यदि युवती किसी का नाम नहीं लेती या पहचानने से इनकार करती है, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार को पूजा सामग्री—जैसे खस्सी (बकरा), चावल आदि—देने का दंड दिया जाता है। इसका उद्देश्य गांव की पवित्रता की पुनः स्थापना होता है।
ऐसे मामलों में बच्चे का नामकरण और गोत्र ‘जोग मांझी’ के गोत्र के आधार पर कर दिया जाता है। यदि कोई लड़का लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, तो पारंपरिक विवाह की अनुमति दी जाती है, और उस संतान को उस लड़के का गोत्र दिया जाता है। बदले में लड़की के पिता उस लड़के को कुछ संपत्ति या धनराशि प्रदान करता है।
3. बिटलाहा प्रथा—दंड न मानने की स्थिति में सामाजिक बहिष्कार
यदि किसी व्यक्ति को अपराधी करार दिया जाता है और उसे पारंपरिक पंचायत द्वारा दंड भी निर्धारित किया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति दंड स्वीकार नहीं करता, तो उसे ‘बिटलाहा’ घोषित कर दिया जाता है। यह स्थिति व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार की सूचक होती है, जहां उसे गांव के सार्वजनिक और सामाजिक कार्यों से वंचित कर दिया जाता है। जब तक वह दंड स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका पुनः समाज में स्थान नहीं बनता।
4. सामाजिक निर्णयों में संवेदनशीलता और न्यायिक दृष्टिकोण
सामान्यतः गांव के लोग एक-दूसरे की परिस्थिति और पृष्ठभूमि से भलीभांति परिचित होते हैं। इसलिए वे अपने निर्णयों में न्याय और सहानुभूति दोनों का समावेश करते हैं। लेकिन गंभीर अपराधों के मामलों में यह व्यवस्था किसी प्रकार की ढील नहीं देती।
बिटलाहा’ प्रथा: सामाजिक बहिष्कार की पारंपरिक व्यवस्था
झारखंड के आदिवासी समाज में यदि कोई व्यक्ति या परिवार पारंपरिक पंचायत द्वारा निर्धारित दंड को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उस पर ‘बिटलाहा’ की प्रक्रिया लागू की जाती है। यह सामाजिक बहिष्कार की एक संगठित और सांस्कृतिक विधि है, जो समाज में अनुशासन बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम रही है।
इस प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब परगनैत की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है कि आरोपी व्यक्ति या परिवार को समाज से अलग किया जाएगा। निर्णय के पूर्व संबंधित गांव, मांझी और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है। आरोपित व्यक्ति को पहले समझाने की कोशिश की जाती है—गांव-गांव के प्रतिनिधि जाकर उससे वार्ता करते हैं। यदि इसके बावजूद भी वह व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता या दंड नहीं देता, तो फिर पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि एक दिन, तारीख और स्थान तय कर सार्वजनिक रूप से ‘बिटलाहा’ की घोषणा करते हैं।
इस औपचारिक बैठक में आरोपी के गांव के मांझी को भी बुलाया जाता है। मांझी आम तौर पर यह कहता है कि, “यह व्यक्ति हमारी प्रजा है, लेकिन यदि दोषी है तो मैं समाज को उसे बिटलाहा करने की अनुमति देता हूँ। परंतु मेरी यह विनती है कि उसके परिवार के अलावा अन्य किसी को हानि न पहुंचाई जाए।”
इसके बाद प्रतीकात्मक अपमान की प्रक्रिया शुरू होती है—सबसे पहले आरोपी परिवार का ‘चूल्हा’ तोड़ा जाता है। संताल समाज में यह अत्यंत अपमानजनक माना जाता है। इसके बाद कभी-कभी सामाजिक आक्रोश इतना तीव्र होता है कि आरोपी परिवार की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, मवेशी हांक दिए जाते हैं, घर उजाड़ दिया जाता है। ये घटनाएं खासकर यौन अपराधों जैसे बलात्कार या यौन शोषण के मामलों में ज्यादा देखी जाती हैं।
यह प्रथा भले ही कठोर लगे, लेकिन समाज के भीतर अनुशासन और सामाजिक न्याय के संरक्षण में इसका विशेष स्थान रहा है।
जमीन-जायदाद के विवादों में पारंपरिक नेतृत्व की भूमिका
संताल समाज में भूमि केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानी जाती है। ऐसे में जमीन को लेकर विवादों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये विवाद चाहे परिवार के भीतर हों या गांवों के बीच, इनका समाधान पारंपरिक नेतृत्व संरचना—मांझी से लेकर परगनैत तक—के माध्यम से किया जाता है।जब जमीन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका उल्लेख पहले गांव के मांझी से किया जाता है। मांझी शिकायत प्राप्त होते ही गांव के अन्य पदधारियों और आम ग्रामीणों की बैठक बुलाते हैं। बैठक में दोनों पक्षों की बातें और गवाहों के बयान ध्यानपूर्वक सुने जाते हैं। इसके बाद मांझी, जोग मांझी, नायके, कुड़ाम नायके जैसे पदधारी और भग्दो प्रजा मिलकर विचार-विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। यह निर्णय प्रायः सामूहिक सहमति से होता है। यदि किसी पक्ष को मांझी का फैसला स्वीकार नहीं होता, तो वह मामले को अगले स्तर यानी देश मांझी (या मोड़े मांझी) के पास ले जा सकता है। यदि वहां भी समाधान न हो, तो अंततः मामला परगनैत तक पहुंचता है। पूर्वकाल में, जब न्यायालय की व्यवस्था नहीं थी, तब परगनैत का निर्णय अंतिम माना जाता था। वह सामाजिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर मान्य होता था।
निष्कर्ष
संथाल समाज की यह पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था एक तरह की ग्राम कैबिनेट है, जो प्रशासन, न्याय, सुरक्षा और संस्कृति को साथ लेकर चलती है। यह न केवल समाज को संगठित रखती है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाती है। आज भी कई क्षेत्रों में यह व्यवस्था सरकारी तंत्र के पूरक के रूप में काम करती है।
इसे भी पढ़ें