झारखंडी भाषा साहित्य एवं संस्कृति पर ग्रंथ – लेखन एवं शोध – प्रकाशन की अनवरत प्रक्रियाएँ चल रही है उससे सुखद अनुभूति स्वाभाविक है। खास कर खोरठा भाषा (Khortha bhasa) साहित्य पर जो काम हो रहे हैं उससे लगता है कि खोरठा भाषा की व्यापकता और उपादेयता में वृद्धि हो रही है। यह कारण है कि न सिर्फ स्कूलों, कालेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में इसके अध्ययन, अध्यापन की व्यवस्था की गयी है बल्कि झारखंड राज्य के कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसे विषय के रूप में शामिल किया गया है। झारखंड की नौ मान्यता प्राप्त भाषाओं में खोरठा भाषा (Khortha bhasa) को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। खोरठा की विकास यात्रा का ठहराव इतने पर ही नहीं हो सकता। उसे और गति और उर्जा मिले इसके लिए लेखकों, कवियों, साहित्यकारों, शोधार्थियों, जिज्ञा विद्यार्थियों एवं बुद्धिजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कड़ी में मैं डॉ. आनन्द किशोर दाँगी अपने ब्लॉग पर खोरठा भाषा के ब्यापक रूप से लिखे है। जिससे स्कूलों, कालेजों, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, प्रतियोगिता परीक्षा जैसे JPSC, JSSC में इसके अध्ययन, अध्यापन में काफी सहायता होगा। मैं इस ब्लॉग पर खोरठा भाषा के विश्लेषणात्मक अध्ययन चर्चा किया गया हैं।
यह भाषा झारखण्ड राज्य के कर्क रेखा से उतरी क्षेत्रों की मातृभाषा खोरठा है । इस भाषा की भौगोलिक स्थिति को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए इसकी व्यापकता को दर्शाया गया है । यह तारीफे काबिल है । दूसरी बड़ी बात यह है कि खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास की गति साठ के दशक से आयी वह अनवरत जोर पकड़ती गई जो मूक्ति दायी प्रवाह साबित हुई। नव जागरण की चेतना , नयी भाव भूमि , नया परिवेश और नये वातावरण में उन्मूक्त सांस लेती हुई खोरठा भाषा – साहित्य समृद्ध होती चली गयी । साठ के दशक से तो खोरठा साहित्य में नवीन सौन्दर्य बोध एवं नूतन संवेदना मुखर हुई जिसमें यर्थाथवाद, अस्मिता की पहचान शोषण से मुक्ति की आकांक्षा आदि भाव प्रस्फुटित होते चली गई। खोरठा साहित्य के सभी विधाओं में रचना मिलने लगी। खोरठा विषय के सभी विधाओं में पुस्तक मिल जाएंगे, किन्तु इंटरनेट पर कोई पढ़ना चाहे तो इस विषय पर रचना नगण्य ही मिलेगा। मैं ऐसी कमी को पाटने के लिए इस ग्लोबलाइजेशन युग मे अपने ब्लॉग के माध्यम से खोरठा भाषा को आप तक पहुचाने का बीड़ा उठाया हुँ।
खोरठा भाषा – साहित्य का सामान्य परिचय
( क ) खोरठा भाषा का उद्भव और विकास
खोरठा भाषा का उद्भव :– खोरठा भाषा झारखण्ड प्रान्त के उस भाषा विशेष का बोध कराता है, जो उतरी छोटानागपुर, पलामू ओर संथाल परगना के पन्द्रह जिलों के लोगों की मातृभाषा है । साथ ही झारखण्ड में सदियों से सदान और आदिवासी साथ – साथ रहते आये हैं, खोरठा भाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य एक उनके बीच सम्पर्क भाषा के रूप सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहने के कारण उसे सर्वदा आपस में विचार विनिमय करना ही पड़ता है और भाषा मनुष्य के विचार विनिमय का सबसे उत्तम और सरल माध्यम है। वह सिर हिलाकर, हाथों से इशारा करके या आंखों को दबाकर अपने भाव प्रकट करने का प्रयास करता है। वास्तव में मनुष्य द्वारा अपनी पाँच ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त पाँच अनुभूतियों- गंध, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि और कर्ण मे से किसी के भी माध्यम से अपने भाव प्रगट किये जा सकते हैं। – भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से जीव सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं । भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है , जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अतः भाषा वह है , जिसे बोला जाय । भाषा विचार विनिमय का माध्यम है तथा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्यों के उच्चारणवयवों से निस्सृत ध्वनि समष्टि है । “ सभी भाषाओं की अपनी पहचान है , लेकिन मातृभाषा ही हमारी असली पहचान है । ‘ ‘ भाषा मनुष्य का अनूठा अविष्कार है। यह मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक है। सबसे पहले इसने मानव को पशु से अलग किया । इसने विभिन्न किस्म के मानवीय अनुभवों और ज्ञानों को न केवल एक – दूसरे के बीच वरन् पीढ़ी दर पीढ़ी उक्त अनुभवों और ज्ञानों को हस्तांतरित करने की क्षमता प्रदान की । मानव के चतुर्दिक विकास का मार्ग खोलने वाली यह भाषा हीं तो रही है। आज भाषा के बदौलत मानव सृष्टि का अपराजेय योद्धा बना हुआ है । भाषा को ही पूरी दुनिया को वैश्विक गांव बनाने का श्रेय है तो पूरी दुनिया को खण्ड – खण्ड बांटने और रक्तपात कराने का कराने का श्रेय भी इसे इसे मेंं आता। समाज का हर गतिविधि भाषा के द्वारा अभिव्यक्त और निर्देशित होती है । समाज का हर्ष और विषाद् , उमंग, आनन्द और उत्साह, समाज का अभिमत, सार कुछ भाषा का सहारा पाकर ही अभिव्यक्त होता है । किसी भी भाषा की उत्पति कब और कैसी हुई इसका प्राचीनतम काल से ही विचार होता आया है । सर्वप्रथम यूनानियों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। भाषा उत्पति के विभिन्न सिद्धांतों में निम्नलिखित सिद्धांत है
- दैवी उत्पति सिद्धांत,
- विकासवादी सिद्धांत
- धातु सिद्धांत निर्णय
- सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत
- इंगित सिद्धांत संगीत
- सिद्धांत सम्पर्क सिद्धांत
विद्वान उपरोक्त आधार पर भाषा की उत्पति के संबंध में अपने तर्क दिये। किन्तु अन्ततः यही कहा जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति भावभिव्यंजना अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से ही हुई है । ये सभी सिद्धांत भी भाषा के विकास में सहायक हुए । इस संसार में बारह – तेरह भाषायी परिवार है। जैसे- द्रविड़, चीनी, हेमेटि , सेमेटिक , अग्नेय युराल , आस्टाईक , अमरिकी , इंडियन , सुडानी , बुश्मैनी , जापानी , कोरियाई , भारोपीय इत्यादि । इस संसार में इस भाषा परिवार के लगभग 2769 भाषाएँ एवं बोलियाँ हैं और भारत में 1952 मातृभाषाएँ तथा 187 भाषाएँ हैं । भारत में इतनी भाषाओं का होना यहाँ विभिन्न काल खंडों में अनेक नृजातीय समूहों का आगमन हुआ। समूह यहाँ आकार यहीं के हो गये , अतः उन्होंने अपने साथ अपनी भाषाओं की भी भारतीय भाषिक परिदृश्य पर उपस्थिति दर्ज करा दी । ये इस प्रकार वर्तमान भाषिक परिदृश्य पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी । इस प्रकार वर्तमान भारत की विभिन्न भाषाएँ भारत आने वाले विभिन्न नृजातीय समूहों से सम्बन्धित विभिन्न भाषायी परिवार के साथ साम्य रखती है । इतना ही नहीं , वर्षों से विभिन्न प्राचीन भाषाओं के बीच आपसी अंतक्रियाएँ भी होती रही, जिससे अनेक भाषाओं तथा बोलियो की उत्पत्ति हुई है।उसमेंं आर्य भाषा परिवार केे सदानी भाषा खोरठा भी एक है।
भरत में चार भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है । पहला इंडो यूरोपीय या भारोपीय दूसरा द्रविड़ परिवार , तीसरा आस्ट्रिक परिवार और चौथा चीनी तिब्बती। खोरठा भाषा, भारत के चार भाषा के भारतीय आर्य भाषा के इंडो आर्य के पूर्वी भाग के अन्तर्गत सदानी भाषा का अंग है। यह झारखण्ड राज्य के कर्क रेखा से उत्तरी क्षेत्रों की मातृभाषा है । इस भाषा की भौगोलिक स्थिति 23 58’10 ” से 25 19′ 15 ” उतरी अक्षांश तथा 83 20’50 ” से 88 ° 41’40 ” पूर्वी देशान्तर में स्थित क्षेत्रों की मातृभाषा है। ” झारखण्ड में खोरठा भाषा उत्पति के संबंध में विद्वान अलग – अलग मंतव्य दिये हैं। ‘ ए.के. झा ‘ ने इसके उत्पति के संबंध में कहा है- “ भाषा की उत्पति अति प्राचीन काल से है , जब खोष्टी लिपि का प्रचलन था और इस भाषा की उत्पति खोष्ठी लिपि से हुआ है। ‘ कृष्ण चन्द्र आला ‘ जी के अनुसार “ खोरठा शब्द की उत्पति खरठा से मानते हैं । खरटा शब्द का अर्थ प्राकृत होता है और खोरठा भाषा प्राकृत ध्वनि से बना खरोष्ठी लिपि और खोरठा भाषा के बीच के संबंधों के बारे में भाषा विज्ञानी कृष्ण चन्द्र दास आला अपनी पुस्तक ” खारठा भाखा गर्हन ” में लिखते हैं ” खरटाक आवगा विदुवान सब हंकद हथ जे आइरज भाखाक आगु हिंया खरेष्टी भाखा हेलए भाखा खोरठा बनल।ओखनिक मत खरोष्ठी ले खलोठी , खरोष्ठी , खोरठा , खोरठा फइर खोरठा बनल हइ । कहेक माने खरोष्ठी आर खोरठा दुयो एक लागइ , दुइ नांञ् । खरोष्ठी अखरावेक टावान पावा हइ आइझ ले साढ़े छव हजार बछर आगु से। जइन गरंथ ‘ पन्नवणा सुत्र ‘ ए खरोष्ठी उखरान आंकलन करल गेल हइ । ” ” खोरठा भाषा की उत्पति के संबंध में ‘ श्री शिवनाथ प्रमाणिक ‘ खोरठा क्षेत्र में उपलब्ध लोक गीतों , दन्तकथाओं , लोककथाओं को आधार बनाकर इसकी उत्पति आर्यों के आगमन के पूर्व मानते हैं। उनका तर्क है – ” खोरठा क्षेत्र में उपलब्ध लोकगीतों , दन्तकथाओं , लोककथाओं , कहावतों , लोक मान्यताओं , विश्वासों तथा प्रचलित प्रथाओं के गहन अध्ययन एवं चिन्तन करने के पश्चात् यह प्रमाणित होता है । कि खोरठा भाषा एक बोली के रूप में प्रागैतिहासिक काल में विद्यमान थी । उदाहरणार्थ एक द्रविड़ परिवार ( विरहोर ) के एक गीत को लें आसना पातेक दोसना , कोरइया पातेक दोना , दोने – दोने मांड परसे , हिले कानेक सोना । और एह डींडा ओह डींडा चल पोखर पींडा आइन देबो चीटा माटी लेस देबो पींडा। 17 इस तरह कहा जा सकता है कि भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व खोरठा आदिमवासियों की बोली के रूप में प्रचलित थी । आर्यों के आगमन के पश्चात् उन्होंने भी इसे सहृदय अपनाया । कालान्तर में खोरठा सामन्तों , जमीनदारों , राजा , महाराजाओं पुष्ट और समृद्ध होती गई । तथा ठाकुर घरानों के रंगमहलों में यह लोकगीत के रूप में मनोरंजनार्थ और अधिक सारे भाषा विज्ञानी एक मत रखते हैं और मानते हैं कि भारत में आर्यों के प्राकृत भाषा आने से पूर्व यहाँ की भाषा प्राकृत थी। इसी प्राकृत से सारे भाषाओं का सृजन हुआ है । ही मागधी , अर्द्धमागधी , पाली इत्यादि भाषाओं का विकास हुआ। यह हुए , जिनमें 6 ठी शताब्दी में चरमोत्कर्ष पर था । इस काल में अनेक सामाजिक , धार्मिक आन्दोलन प्रमुख जैन , बौद्ध , भागवत आजीवक इत्यादि हैं । इन धर्मों को प्रचार – प्रसार का माध्यम द्वितीय प्राकृत भाषा ही था। झारखण्ड में इन धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ । दूसरी ओर मगध सम्राज्य का सम्राज्य विस्तार तथा मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक द्वारा कलिंग आक्रमण तथा वाणिज्य – व्यपार के द्वारा इन क्षेत्रों में आर्य जाति के लोग बसने लगे । यहाँ सदियों से आदिवासी समुदाय रह रही थी। उसकी अपनी भाषा थी । उपरोक्त कारणों से लोग उनके साथ रहने लगे । दोनों के बीच सम्पर्क भाषा के रूप में इस नये भाषा का विकास हुआ, जिसे सदानी भाषा कहते हैं। सदानी भाषाओं पर आदिवासी भाषा, सीमावर्ती राज्यों की भाषा, जैसे- बंगला, मैथली, भोजपुरी, उड़िया इत्यादि के प्रभाव से नये भाषा का जन्म हुआ, जिसमें खोरठा पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली है ।
खोरठा भाषा का नामकरण :-
खोरठा शब्द की व्युत्पति को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है । खोरठा शब्द की व्युत्पति के संबंध में खोरठा भाषा के विद्वान ए . के . झा का मत है कि खोरठा शब्द की उत्पति भारत की प्राचीन लिपि खरोष्ठी से हुई है। ध्वनि परिवर्तन के कारण खरोष्ठी से खोरठा बना – खरोष्ठी > खरोठी > खरोष्ठी > खारोठी> खरोटा। खोरठा डॉ. जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण करते हुए पूर्वी मघी की सीमावर्ती बोली को खोटटा कहा है। दूसरी ओर खोरठा भाषा के एक और विद्वान कृष्ण चन्द्र दास आला जी ने अपनी पुस्तक “ खरा भाखा गर्हन ” में लिखा है – ” खोरठा शब्द खरोष्ठी से उत्पन्न नहीं हुई है । वरन् यह खरठा शब्द से बना है , जिसका अर्थ प्रकृति होता है । चूंकि खोरठा प्रकृति मूलक भाषा है , अतः खरठा से इसकी व्युत्पति ज्यादा तर्कपूर्ण है। ” उनके मत में ही खरठा उच्चारण दोष , विशेषतः बंगाली समुदाय के उच्चारण के कारण खोरठा बन गया । → → खरोठा खोरठा खलोटी → कुछ लोग खोरठा शब्द को बंगाल के खोट्टा ( विकृत बंगला ) शब्द से बना हुआ मानते हैं। डॉ. बी. एन. ओहदार, कृष्ण चन्द्रदास ‘ आला ‘ के मत से सहमत नहीं हैं। उनका तर्क है कि खरठा नामक कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ प्रकृति से होता है। अतः खोरठा की जगह खरठा कभी स्वीकार्य नहीं है। विशेष बात तो यह भी है कि खोरठा शब्द अति लोकप्रिय हो चुका है। इस संबंध में डॉ . बी . एन . ओहदार लिखते हैं – ” खोरठा और खरोष्ठी में ध्वनिगत समानता देखकर ऐसा लगता है कि खरोष्ठी लिपि का अविष्कार जिस भाषा विशेष के लिए हुआ होगा वह या तो खोरठा या खरोष्ठी से मिलती जुलती भाषा रही होगी । इस तरह यह कहा जा सकता है कि खोरठा और खरोष्ठी का नाम साम्य वस यूँ हीं नहीं है , बल्कि इसका तार्किक आधार भी है । ” उन्होंने खोरठा भाषा को किसी न किसी रूप में पालि , द्वितीय प्राकृत तथा अपभ्रंश से जुड़ा मानते हैं । इस संबंध में उनके ठोस तर्क हैं । पालि भाषा की ध्वनिगत विशेषताएँ खोरठा विशेषताओं से शत प्रतिशत साम्य रखती हैं । प्राकृत की अनुकरणात्मक और अनुरणात्मक ध्वनियों की तरह खोरठा में भी ऐसी ध्वनियाँ प्रचुर मात्रा में हैं । अपभ्रंश भाषा में ‘ उकार ‘ ध्वनियों की बहुलता है , किन्तु खोरठा में आकर ध्वनियों की बहुलता है। काल और स्थान के कारण इस तरह के भेद की संभावना है। इस प्रकार कहा जा सकता है , कि खोरठा भाषा का नाम खोरठा , प्राचीन लिपि खोष्टी से ही नाम पड़ा होगा । खोष्ठी लिपि के कुछ विशेषताएँ वर्तमान में खोरठा भाषा में पाई जाती है , जैसे 37 मात्रा का प्रयोग ह्रस्व ध्वनि की प्रधानता , मध्यस्वरागमन की प्रवृति इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं, कि खोष्ठी लिपि का प्रयोग जिस भाषा विशेष के लिए हुआ होगा वह खोरठा भाषा से मिलती – जुलती भाषा रही होगी। इस कारण इसका नाम खोरठा पड़ा ।
( ख ) खोरठा भाषा का क्षेत्र विस्तार , जनसंख्या एवं विशेषता
खोरठा भाषा का क्षेत्र विस्तार :-
खोरठा भाषा झारखण्ड के सदानी भाषाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि अन्य सदानी भाषाओं की अपेक्षा इसका क्षेत्रफल तथा बोलने वालों की संख्या अधिक है, साथ ही इस भाषा की साहित्य भी प्राचीन है। यह झारखण्ड राज्य के कर्क रेखा से उत्तरी क्षेत्रों की मातृभाषा है। अर्थात् 15 जिलों की मातृभाषा है। भाषा की भौगोलिक स्थिति 23½2 ° 58’10 ” से 25 ° 19’15 ” उत्तरी अक्षांश तथा 83 2050 ” 88 ° 4’40 ” पूर्वी देशान्तर में स्थित क्षेत्र आते हैं।
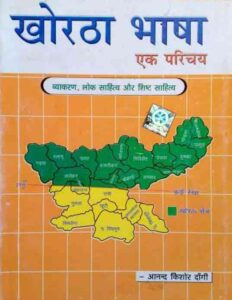
खोरठा भाषा के राजनैतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन के पश्चात् यह बात सामने आती है। सम्पूर्ण पृथ्वी का खोरठा क्षेत्र गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भू – भाग है तत्पश्चात् अनेक पुरानों में वर्णित है ।
अयः पात्रे पयः पानं , शाल पत्रे च भोजनम् ।
श्यनं खर्जुरी पत्रे , झारखण्डे विहियते ।।
“ यह श्लोक प्राचीनता को सिद्ध करता है। मनोरम हरीतिमा से युक्त यह धरती आदि काल से प्राकृतिक सुषमाओं में परिपूर्ण है। कलकल निनादिन दामोदर, बराकर, संकरी, अजय, मयूराक्षी नदियों की अजस जलधाराएँ युग – युग से इस धरती में प्रवाहित हैं । इसके अतिरिक्त इनकी असंख्या उपशाखाएँ सहायिकाएँ , जलप्रपात , गर्म कुंड आदि जल की अक्षय निधियाँ हैं। जंगलों में महुआ, शाल, शीशम, करंज, अर्जुन, महोगनी, आसन, करम कुसुम, पलाश , बैर आदि कीमती वृक्ष हैं । इनके अलावे इन जंगलों में रोग निवारक फल – फूल , जड़ी – बूटी बहुताय में पाये जाते हैं । नानाविध पशु – पक्षी जंगलों में आश्रय किये विहार करते हैं । झारखण्ड क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत पासरनाथ खोरठा भू – भाग का गौरव है । इसके अलावे खरगा, चुटुपालू , सेंवाती , कैल्हुआ इत्यादि सुंदर पहाड़ियाँ बिराजमान हैं । आहार – विहार के लिए घने जंगल पहाड़ – पहाड़ियाँ , असंख्य जलश्रोत जहाँ मौजूद हों , वहाँ मानव का आश्रय स्वभाविक हैं । यही कारण है कि यह स्थान कभी निर्जर नहीं रहा , जिसका प्रमाण हजारीबाग का महुदी पहाड़ , दामोदर और संकरी नदियों के किनारे यत्र – तत्र सर्वत्र बिखरे और उपेक्षित मानव बस्तियों के भाग्नावशेषों के अवलोकन करने से पता चलता है । इन भग्नावशेषों की चर्चा हजारीबाग , मानभूम , राँची आदि गजेटियरों में है । इस प्रकार हम देखते हैं कि खोरठा भाषा का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है । इसे सदान परिवार यथा कोईरी , दांगी , कुर्मी , कुम्हार , धोबी , राजपूत , बनिया , तेली , ब्राह्मण , महली , केवट , मुस्लिम इत्यादि के अलावे आदिवासी परिवार , बिरहोर , करमाली , मुंडा , संथाल , उराँव आदि भी दैनिक जीवन में सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं । यही कारण है कि सम्पूर्ण झारखण्ड का सम्पर्क भाषा बन गई है।
खोरठा भाषा के क्षेत्र विस्तार काफी विस्तृत हैं। पन्द्रह जिलों में पूर्णतः खोरठा भाषा बोली जाती है और आंशिक रूप से खोरठा भाषा के सीमावर्ती जिले के कुछ क्षेत्र हैं , जैसे- राँची के ओरमांझी , सिकदरी , मनातु , खलारी , वर्मा , जुवला , गोरीड़ह इत्यादि , लातेहार जिला के भटचैरा , बालूमाथ , सालवे , चकली मुरपा , टोरी , बालूमाथ , फूलसू इत्यादि । पूर्णतः खोरठा बोले जाने वाले जिले – चतरा , कोडरमा देवघर, गिरिडीह ,बोकारो ,साहेबगंज, पाकुड़ ,गोड्डा, जामताड़ा ,धनबाद ,रामगढ़ ,हजारीबाग , पलामू, गढ़वा, दुमका। आंशिक रूप से बोले जाने वाले जिले -राँची ( ओरमांझी , सिकदरी , मनातु , खलारी , जुवला इत्यादि ) लातेहार ( भटचैरा , सालवे , चकली मुरपा इत्यादि )।
खोरठा भाषा क्षेत्र के 15 जिलों में प्रखण्डवार ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या कितनी है । शोध से स्पष्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या अपने आम जीवन में अपनी मातृभाषा खोरठा का ही प्रयोग करते हैं । इन क्षेत्रों में शहरी जनसंख्या को छोड़ दिया जाय तो खोरठा भाषा बोलने वालों की संख्या अन्य सदानी भाषाओं से अधिक है ।
खोरठा भाषा का क्षेत्रीय स्वरूप
खोरठा भाषा 487558.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बोली जाती है और 2011 की जनगणना के आधार पर 40412198 लोगों की मातृभाषा है । जब इतने विशाल क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है तो कुछ भिन्नता स्वभाविक है । यह कहावत है ” तीन कोस पर पानी बदले सात कोस पर वाणी ” यहाँ चरितार्थ होता है ।शोध से स्पष्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या अपने आम जीवन में अपनी मातृभाषा खोरठा का ही प्रयोग करते हैं । इन क्षेत्रों में शहरी जनसंख्या को छोड़ दिया जाय तो खोरठा भाषा बोलने वालों की संख्या अन्य सदानी भाषाओं से अधिक है । । इस भिन्नता के आधार पर खोरठा भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को पाँच भागों में बांटा जाता है – 1 . सिखरिया 2 गोलवा 3. देसवाल परनदिया5 संथाल परगनिया
1 . सिखरिया- सिखरिया जैना मोड़ से प्रारम्भ होकर पूर्व में झारखण्ड प्रदेश की सीमा तक तथा दक्षिण में खोरठा कुरमाली की सीमा तक हरनाद , खैराचातर , मंइजरा , खोरठा के क्षेत्र को छूता है । कसमार , बहादुरपुर , खूंटा और बेरमो तक के क्षेत्र में इसका फैलाव है , जो बोलवारी इसका विस्तार है ।
2. गोलवारी गोला गोलवारी गोला से पूर्व और कसमार के आसपास के इलाके तक – पलामू जिले की आखरी सीमा तक इसका विस्तार है ।
3. देसवाली- देसवाली पतरातू प्रखण्ड के सियाड़ी से प्रारम्भ होकर पश्चिम में पलामू ज़िला के आखरी सीमा तक इसका विस्तार है
– 4. परनदिया – दामोदर नदी के उत्तर कोडरमा जिले की उत्तरी सीमा तक 25 इत्यादि जिले आते हैं । इसका प्रसार है । यह एक विशाल क्षेत्र है । पूरा गिरिडीह , कोडरमा , चतरा , हजारीबाग
5. संथाल परगनिया – खोरठा क्षेत्र के उत्तर पूरब का भाग जिसे संथाल परगना कहा जाता है , इस भाषा का क्षेत्र है । इस पर मैथिली और अंगिका का प्रभाव प्रत्येक भाषा का अपना एक केन्द्रीय रूप होता है ।
इस केन्द्रीय क्षेत्र में व्यहृत भाषा मोटा – मोटी तौर पर पूरे भाषा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। खोरठा भाषा का भी अपना एक केन्द्रीय रूप है । खोरठा के एक वरिष्ठ विद्वान ‘ श्री ए.के. झा ‘ के अनुसार खोरठा का केन्द्रीय रूप और क्षेत्र है- “ दामोदर नदी आर पारसनाथ पहार के सटल आर ओकर बावें दहइने खोरठा रूप के केन्द्रीय रूप मानल नाइ पारे , काहे कि ई झारखंडेक संस्कृति के उन बेजोड़ चेतना के छाप मिल हे जकर चलते आज संस्कृति से झारखंडेक संस्कृति के भिनु रूपे देखल जाइ पारे । ई ठेठ छेतरेक केन्द्रीय खोरठा रूपेक केन्द्र राइख के अनुसार भिनु छेतरीय रूप गुलाक विसेसताक समइट के एगो केन्द्रीय आर मानक रूप के स्थापना करल नाइ पारे । ”
वर्तमान समय में खोरठा भाषा झारखण्ड के सदानी भाषा समूह की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय भाषा के रूप में जानी जाती है । इसे शिष्ट भाषा की मान्यता प्राप्त हो चुकी है तथा झारखण्ड सरकार इसे द्वितीय राजभाषा के रूप में भी स्थान दे दिया है , किन्तु दुर्भाग्य है कि यह भाषा अपनी लोकभाषा के आवरण और आच्छादान से स्वयं को निकाल नहीं पाई है । इसका कोई निश्चित मानक रूप तैयार न हो सका है । इस भाषा क्षेत्र के उपक्षेत्रों के भाषा – भाषियों की भावभिन्नता के कारण इसका सर्वग्राह्य मानक रूप प्रतिष्ठित न हो सका है । हलांकि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के मानकीकरण का प्रथम प्रयास 1984-85 ई . में किया गया था , जिसमें कुछ निर्णायक रूप सामने आया । समय – समय पर इस भाषा के मानकीकरण पर कार्यशाला , सम्मेलन का आयोजन हो रहा है , किन्तु एक सर्वमान्य विचार सामने नहीं आ पाया है ।
खोरठा भाषा की विशेषता
हर किसी भाषा की अपनी खास विशेषता होती है, जो अन्य भाषाओं से अलग करती है। खोरला भाषा इतने विशाल क्षेत्र में प्राचीन काल से बोली जा रही है , तो स्वभाविक है कि इस भाषा की अपनी खास विशेषता होगी, जो इस प्रकार है-
- अर्द्ध विवृत अग्रस्वर ‘ ए ‘ का हरस्व प्रयोग
- अछविकृत अवस्वर ऐ का और पश्चस्वर औ का उच्चारण नहीं किया जाना
- महाप्राणीकरण की प्रवृति
- घोषीकरण- आयोषीकरण का आप प्रयोग
- ह्रस्व ध्वनि का अत्याधिक प्रयोग
- सानुनासिकता स्वर सानुनासिक होता है ।
- मध्यस्वरागमन की प्रवृति
- संयुक्त व्यानियों का प्रयोग नहीं किया जाता है
- दन्तय व्यानि तालव्य ध्वनि में परिवर्तन तालव्य ध्वनि दन्त ध्वनि में परिवर्तन
- पार्श्विक ध्वनि तुठित ध्वनि में परिवर्तन
- खोरठा के वाक्य क्रिया केन्द्रित होता है ।
- कर्म प्रधान वाक्य होते हैं ।
- खोरठा में अन्य भाषाओं की तरह लींग बोधक नहीं होता है ।
- शब्द के क्रम बदलने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।
- इस भाषा की अपनी व्याकरणिक विशेषता है ।
- इस भाषा की अपनी मानक रूप है ।
- खोरठा भाषा की अपनी कारकीय विभक्ति है जो अन्य भाषा से अलग करती है ।
- सबसे बड़ी विशेषता इसके ठेठ शब्द है ।
इन्हें भी पढ़ें
| ई- श्रमिक कार्ड योजना (e-SHRAM Portal) |
नोट ;-उपरोक्त विशेषता का विश्लेषण विस्तृत रूप में खोरठा व्याकरण में उल्लेख किया जायगा ।